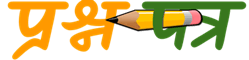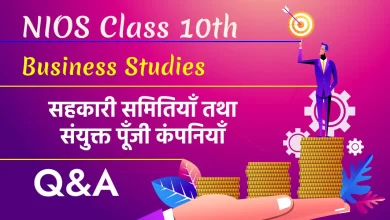Class 12th History Chapter 3. बंधुत्व, जाति तथा वर्ग

Class 12th History Chapter 3. बंधुत्व, जाति तथा वर्ग
NCERT Solutions For Class 12th History Chapter- 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज :– जो उम्मीदवार 12 कक्षा में पढ़ रहे है उन्हें History सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है .हमने हमारी वेबसाइट पर 12th कक्षा History सब्जेक्ट के सभी चेप्टरों सलूशन दिए है .यहां पर हमने एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास अध्याय 3 (बंधुत्व, जाति तथा वर्ग) का सलूशन दिया गया है .इस NCERT Solutions For Class 12th History Chapter 3 Kinship, Caste and Class की मदद से विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकता है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है. इसलिए आप Ch.3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के प्रश्न उत्तरों ध्यान से पढिए ,यह आपके लिए फायदेमंद होंगे. इसलिए नीचे आपको एनसीईआरटी समाधान कक्षा 12 इतिहास अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग दिया गया है ।
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 12 |
| Subject | HISTORY |
| Chapter | Chapter 3 |
| Chapter Name | बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज |
| Category | Class 12 History Notes In Hindi |
| Medium | Hindi |
पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न (Textual Questions)
उत्तर- पितृवंशिकता से अभिप्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। विशिष्ट परिवारों में शासक परिवार तथा धनी लोगों के परिवार शामिल हैं। इन परिवारों में पितृवंशिकता निम्नलिखित दो कारणों से अनिवार्य रही होगी|
1. वंश परंपरा को चलाने के लिए-धर्म सूत्रों के अनुसार वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं, पुत्रियाँ नहीं। इसलिए प्रायः सभी परिवारों में उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की कामना की जाती थी। यह बात ऋग्वेद के एक मंत्र से स्पष्ट हो जाती है। इसमें पुत्री के विवाह के समय पिता कामना करता है कि इंद्र के अनुग्रह से उसकी पुत्री को उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हो।
2. उत्तराधिकार संबंधी झगड़ों से बचने के लिए-माता-पिता नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए कोई झगड़ा हो। राज परिवारों के संदर्भ में उत्तराधिकार में राजगद्दी भी शामिल थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन जाता था। इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को उनके पुत्रों में बाँट दिया जाता था। अत: अधिकतर राजवंश लगभग छठी शताब्दी ई० पू० से ही पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते आ रहे थे हालाँकि इस प्रथा में विभिन्नता थी।
(i) पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी बन जाता था।
(ii) कभी-कभी सगे-संबंधी सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे।
(iii) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियाँ सत्ता का उपभोग करती थीं। प्रभावती गुप्त इसका उदाहरण है।
उत्तर- शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे परंतु कई महत्त्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्गों से भी हुई थी। उदाहरण के लिए मौर्य वंश को ही लीजिए। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह व्यक्त किया गया है कि मौर्य शासक क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न’ कुल का ही मानते हैं। इसी प्रकार शुंग और कण्व, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वास्तव में समर्थन और संसाधन जुटा सकने वाला प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता था।
ब्राह्मण लोग शकों को, जो मध्य एशिया से भारत आए थे, मलेच्छ तथा बर्बर मानते थे परंतु संस्कृत के एक आरंभिक अभिलेख में प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण (मरम्मत) का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परंपरा से परिचित थे।
एक अन्य रोचक बात सातवाहनों के संबंध में है। सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमी-पुत्र सिरी सातकनि ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताने के साथ-साथ अपने आप को क्षत्रियों के अभिमान का हनन करने वाला भी बताया था। उसने यह भी दावा किया था कि उसने चार वर्षों के बीच आपसी विवाह संबंधों पर रोक लगाई है परंतु फिर भी उसने स्वयं रुद्रदमन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए। इन उदाहरणों से स्पष्ट है। कि आरंभिक राज्यों में शासक के लिए जन्म से क्षत्रिय होना अनिवार्य नहीं था।
उत्तर- द्रोण- द्रोण एक ब्राह्मण थे जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। धर्मसूत्रों के अनुसार शिक्षा देना ब्राह्मण का कर्म था। इस प्रकार द्रोण अपने धर्म का पालन कर रहे थे। उस समय निषाद शिक्षा नहीं पा सकते थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया परंतु उससे गुरुदक्षिणा में दाएँ हाथ का अँगूठा ले लेना धर्म के विपरीत था। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने आखिर उसे अपना शिष्य मान लिया। वास्तव में यह उनका स्वार्थ था। उन्होंने अर्जुन को दिए गए अपने वचन को निभाने के लिए ऐसा तुच्छ काम किया। वह नहीं चाहते थे कि संसार में अर्जुन से बढ़कर कोई धनुर्धारी हो।
हिडिंबा- हिडिंबा एक राक्षसिनी थी। राक्षसों को नरभक्षी बताया गया है। उसके भाई ने उसे पांडवों को पकड़कर लाने का आदेश दिया था, ताकि वह उन्हें अपना आहार बना सके परंतु उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। उसने पांडवों को पकड़कर लाने की बजाय भीम से विवाह कर लिया और एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार उसने राक्षस कुल की मर्यादा को भंग किया।
मातंग- चाण्डाल भी अपने को समाज का अंग समझते थे। इसकी पुष्टि मातंग की कथा से होती है। मातंग बोधिसत्व (पूर्व जन्म में बुद्ध) का नाम था। उन्होंने चाण्डाल के रूप में जन्म लिया। उनका विवाह व्यापारी पुत्री दिथ्य मांगलिक नामक कन्या से हुआ और मांडव्य नामक पुत्र का जन्म हुआ। एक बार भिखारी के रूप में मातंग ने मांडव्य से उसके दरवाजे पर भोजन माँगा परंतु उसने उसकी अपेक्षा की।
उत्तर- ऋग्वेद के पुरुषसूक्त’ के अनुसार समाज में चार वर्षों की उत्पत्ति आदि मानव ‘पुरुष’ की बलि से हुई थी। ये वर्ण थे-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन वर्गों के अलग-अलग कार्य थे। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। वे धर्मशास्त्रों के अध्ययन तथा शिक्षण का कार्य करते थे। क्षत्रिय वीर योद्धा थे। वे शासन चलाते थे। वैश्य व्यापार करते थे। शूद्रों का काम अन्य तीन वर्गों की सेवा करना था। इस प्रकार समाज में विषमता व्याप्त थी। इस व्यवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार जन्म था।
बौद्ध अवधारणा इस सामाजिक अनुबंध के विपरीत थी। उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि समाज में विषमता विद्यमान थी परंतु उनके अनुसार यह विषमता न तो प्राकृतिक थी और न ही स्थायी। उन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को भी अस्वीकार कर दिया।
संजय धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहित को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ ….. मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ ….. (और) कुरु वंश के प्रधान भीष्म के। मैं वृद्ध राजा (धृतराष्ट्र) को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनको शुभकामनाएँ देता हूँ….. मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र हैं …… सर्वोपरि मैं उन महामति विदुर को (जिनका जन्म दासी से हुआ है) नमस्कार करता हूँ जो हमारे पिता और माता के सदृश हैं …… मैं उन सभी वृद्धा स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती हैं। जो हमारी पत्नियाँ हैं उनसे यह कहिएगा कि, “मैं आशा करता हूँ कि वे सुरक्षित हैं”….. मेरी ओर से उन कुलवधुओं का जो उत्तम परिवारों में जन्मी हैं और बच्चों की माताएँ हैं, अभिनंदन कीजिएगा तथा हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा ….. सुंदर, सुगंधित, सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएँ दीजिएगा। दासियों और उनकी संतानों तथा वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार कीजिएगा ….. |
इस सूची को बनाने के आधारों की पहचान कीजिए-उम्र, लिंग, भेद व बंधुत्व के संदर्भ में। क्या कोई अन्य आधार भी हैं? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया है?
उत्तर- उम्र, लिंग, भेद तथा बंधुत्व के अतिरिक्त इस सूची को बनाने के कई अन्य आधार भी हैं; जैसे—गुरुजनों के प्रति सम्मान, वीर योद्धाओं, दासियों यहाँ तक कि दासी-पुत्रों के प्रति सम्मान आदि। इस सभी को सूची में उनके सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक विशेष क्रम में रखा गया है।
(1) सर्वप्रथम समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मणों, पुरोहित तथा गुरुजनों के प्रति सम्मान दर्शाया गया है।
(2) दूसरे स्थान पर माता-पिता समान वृद्ध बांधवों के प्रति आदर व्यक्त किया गया है।
(3) इसके बाद अपने से छोटे अथवा एकसमान आयु के बंधु-बांधवों को स्थान दिया गया है।
(4) इसी क्रम में युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन किया गया है।
(5) तत्पश्चात् नारी वर्ग को स्थान दिया गया है। इस क्रम में माताएँ, पत्नियाँ, कुलवधुएँ तथा पुत्रियाँ आती हैं। नारी वर्ग में अंतिम स्थान पर सुंदर-सुगंधित गणिकाओं, दासियों तथा उनकी संतानों को रखा गया है।
(6) अपाहिजों तथा विकलांगों की भी उपेक्षा नहीं की गई है। युधिष्ठिर उन्हें भी नमस्कार करते हैं।
उत्तर- इसमें कोई संदेह नहीं कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है और तत्कालीन भारतीय समाज तथा जनजीवन के सभी पक्षों की एक सुंदर झाँकी प्रस्तुत करता है। इसमें भारतीयों की आत्मा की गहराइयों तक बसी प्रत्येक बात तथा सोच का वर्णन मिलता है। यह महाकाव्य भारतीयों के जीवन पर निम्नलिखित प्रकाश डालता है
1. सामाजिक जीवन
1. चार वर्ण-समाज चार वर्षों में बँटा हुआ था। वर्ण-व्यवस्था अधिक कठोर नहीं थी। लोगों के लिए अपना पैतृक व्यवसाय अपनाना आवश्यक नहीं था। उदाहरण के लिए परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय कहलाए। उस समय के समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त नहीं था।
2. स्त्रियों की दशा-स्त्रियों की दशा अच्छी थी। समाज में उनका बड़ा आदर था। ‘स्वयंवर’ की प्रथा के अनुसार उन्हें अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार था।
3. वीरता का युग-महाभारत का काल वीरता का युग था। युद्ध में वीरगति प्राप्त करना गर्व का विषय समझा जाता था। लोगों का विश्वास था कि युद्ध में मरने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग में जाता है। उस समय निर्बल की रक्षा करना भी बड़ी वीरता का कार्य समझा जाता था।
4. सामाजिक बुराइयाँ-इस काल के समाज में कुछ बुराइयाँ भी थीं। इनमें से जुआ खेलना, बहु-विवाह, शत्रुओं से धोखा करना आदि बातें प्रमुख थीं।
2. राजनीतिक जीवन
1. विशाल साम्राज्य-इस काल में अनेक विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। इन राज्यों में पाँडु, कौशल, पांचाल आदि राज्य प्रमुख थे।
2. राजा की शक्तियाँ-उस समय राज्य का मुखिया राजा होता था। राज्य की सभी शक्तियाँ उसी के हाथ में थीं। इन शक्तियों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी। भले ही शासन कार्यों में राजा को सलाह देने के लिए अनेक मंत्री थे, फिर भी उनकी सलाह मानना राजा के लिए आवश्यक नहीं था। |
3. राजा का जीवन-वीरकाल में राजा बड़े ठाठ-बाठ से रहते थे। उनके महल बड़े शानदार होते थे। वे अनेक उपाधियाँ धारण करते थे। चक्रवर्ती सम्राट बनना उनकी बहुत बड़ी इच्छा होती थी। इस उद्देश्य से वे अश्वमेध यज्ञ रचाया करते थे। उन राजाओं में अनेक अवगुण भी थे। उनके दरबार में अनेक नाचने-गाने वाली नर्तकियाँ होती थीं। शराब पीना और जुआ खेलना आदि बुराइयाँ भी उनके चरित्र में शामिल
थीं।
3. आर्थिक जीवन
1. कृषि—इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। यहाँ तक कि स्वयं राजा लोग भी हल चलाया करते थे। उस समय भूमि बड़ी उपजाऊ थी।
2. पशु-पालन-पशु-पालन लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था। उस समय के पालतू पशुओं में गाय, बैल, घोड़े तथा हाथी मुख्य थे।
3. व्यापार-इस काल में व्यापार काफ़ी उन्नत था। व्यापारियों ने अपने संघ (गिल्ड्स) बनाए हुए थे। उन्हें राज्य की ओर से अनेक सुविधाएँ प्राप्त थीं।
4. अन्य व्यवसाय-पीछे दिए गए व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ लोग बढ़ई, लुहार, सुनार तथा रंगसाजी आदि का कार्य भी करते थे।
4. धार्मिक जीवन
1. नए देवी-देवताओं की पूजा-महाभारत काल में वैदिक आर्यों के देवी-देवताओं के साथ-साथ कुछ नए देवी-देवताओं की पूजा भी की जाने लगी। इनमें से पार्वती, दुर्गा, विष्णु, ब्रह्मा आदि प्रमुख थे।
ऐम बी डी Super Refresher इतिहास-XII)
2. अवतारवाद में विश्वास-इस काल में लोग अवतारवाद में विश्वास रखने लगे थे। राम, कृष्ण आदि को विष्णु का अवतार मानकर उसकी पूजा की जाने लगी।
3. कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म-इस काल में लोग कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में बड़ा विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है।
4. यज्ञों पर बल–महाकाव्य काल में लोग यज्ञों पर बड़ा बल देते थे। यज्ञों की अनेक विधियाँ आरंभ हो गई थीं। राजा लोग यज्ञों के अवसर पर दिल खोलकर दान देते थे।
सच तो यह है कि महाभारत में अन्य महाकाव्यों की भाँति युद्धों, वनों, राजमहलों तथा बस्तियों का बहुत ही सजीव चित्रण है। महाभारत का सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्व है। इस ग्रंथ ने मूर्तिकारों, नाटकों तथा नृत्यकलाओं के लिए विषय-वस्तु प्रदान की
अथवा
महाभारत की मूलकथा के रचयिता कौन थे? महाभारत के पाँचवीं शताब्दी ई० पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी के बीच पूर्ण होने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
अथवा
महाभारत के लेखकों तथा लेखन-काल के विषय में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर-यह संभव नहीं है कि महाभारत का केवल एक ही रचयिता हो। इसकी रचना 500 ई० पू० से लेकर एक हजार वर्ष तक होती रही। फलस्वरूप इसमें नए-नए प्रकरण जुड़ते रहे। दूसरे, इस महाकाव्य में वर्णित कुछ कथाएँ इस काल से भी पहले प्रचलित थीं। इतने लंबे समय तक महाभारत का लिखा जाना किसी एक लेखक का कार्य नहीं हो सकता।।
विभिन्न लेखक– महाभारत के लेखकों के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं
(1) संभवत: इस महाकाव्य की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें ‘सूत’ कहा जाता था। ये लोग क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजयों तथा वीरतापूर्ण कारनामों के बारे में कविताएँ लिखते थे। इन रचनाओं का प्रवाह मौखिक रूप से होता रहा।
(2) पाँचवीं शताब्दी ई० पू० में महाभारत की कथा परंपरा पर ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह समय : था जब कुरु और पांचाल जिनके इर्द-गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। हो सकता है कि राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते हों। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल-पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नए मानदंडों की स्थापना हुई हो जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है।
(3) लगभग 200 ई० पू० से 200 ईसवी के बीच इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और चरण आरंभ हुआ। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना लोकप्रिय हो रही थी। उन्हें श्रीकृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्त्वपूर्ण नायकों में से हैं, विष्णु का रूप बताया जा रहा था। |
(4) समय बीतने पर लगभग 200-400 ईसवी के बीच मनुस्मृति से मिलते-जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। नए जुड़े प्रकरणों के कारण यह ग्रंथ जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर एक लाख श्लोकों वाला हो गया।
(5) साहित्यिक परंपरा में ऋषि वेदव्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है।
उत्तर-आरंभिक समाज में स्त्री-पुरुष के संबंधों की विषमताओं के तीन मुख्य कारण थे
(1) लैंगिक असमानता पितृवंशिक व्यवस्था
(2) स्त्री का गोत्र
(3) संपत्ति का अधिकार।
1. लैंगिक असमानता-आरंभिक समाज पुरुष प्रधान था जो पितृवंशिक परंपरा के अनुसार चलता था। अतः सभी परिवारों में पुत्रों की ही कामना की जाती थी जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाएँ। इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। यही अपेक्षा की जाती थी कि अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर दिया जाए। इस प्रथा को बहिर्विवाह-पद्धति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह था कि प्रतिष्ठित परिवारों की युवा कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बड़ी सावधानी से नियमित किया जाता था ताकि उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इससे कन्यादान अर्थात् विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्त्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया।
2. स्त्री का गोत्र-लगभग 1000 ई० पू० के बाद ब्राह्मणों ने (विशेष रूप से ब्राह्मणों को) गोत्रों में वर्गीकृत किया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के दो नियम महत्त्वपूर्ण थे|
(i) विवाह के पश्चात् स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति के गोत्र का माना जाता था।
(ii) एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे।
परंतु कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनमें इन नियमों का पालन नहीं किया जाता था। उदाहरण के लिए कुछ सातवाहन राजाओं की एक से अधिक पत्नियाँ थीं। इन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों के विश्लेषण से पता चलता है कि उनके नाम गौतम तथा वसिष्ठ गोत्रों से लिए गए थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि इन रानियों ने विवाह के बाद अपने पति-कुल के गोत्र को ग्रहण करने की बजाय अपने पिता के गोत्र को ही बनाए रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियाँ एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह-पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। यह तथ्य वास्तव में एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह-पद्धति अर्थात् बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है। इस विवाह-पद्धति का प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में आज भी है। ऐसे विवाह संबंधों से सुगठित समुदायों को बल मिलता था।
सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम से चिह्नित किया जाता था। इससे तो यह प्रतीत होता है कि माताएँ महत्त्वपूर्ण थीं। परंतु इस निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सातवाहन राजाओं में सिंहासन का उत्तराधिकार प्रायः पितृवंशिक होता था।
3. संपत्ति का अधिकार-मनुस्मृति के अनुसार माता-पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से बँटवारा किया जाना चाहिए। परंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियाँ इस पैतृक संसाधन में भागीदारी की माँग नहीं कर सकती थीं। परंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व होता था। इसे स्त्रीधन (अर्थात् स्त्री का धन) कहा जाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। परंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की अनुमति के बिना पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को गुप्त रूप से इकट्ठा करने से भी रोकती थी।
कुछ साक्ष्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएँ संसाधनों पर अपनी पहुँच रखती थीं, तो भी भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में, स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक स्थिति की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता के कारण ही व्यापक हुई थी।
अथवा
भारतीय उपमहाद्वीप में विविधताओं के कारण हमेशा से ही लोगों के रीतिरिवाज ऐसे रहें जो 600 ई०पू० से 600 ई० तक ब्राह्मणीय विचारों से प्रभावित नहीं हुई थी।” कथन की परख कीजिए।
उत्तर-1. परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। संबंधियों को ‘जाति समूह’ भी कहा जा सकता है। परिवार के संबंधों को स्वाभाविक और रक्त संबंध माना जाता है। कुछ समाजों में भाई-बहन (चचेरे, मौसेरे) से खून का रिश्ता स्वीकार किया जाता है परंतु अन्य समाज इसे स्वीकार नहीं करते हैं।
2. पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके संसाधनों का उत्तराधिकारी बनता है। राजवंश पितृवंशिकता व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। पुत्र के न होने की दशा में एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था।
3. कभी-कभी बंधु-बांधव भी गद्दी के उत्तराधिकारी हो जाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियाँ भी उत्तराधिकारी बन जाती थी जैसे-चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त।
4. प्रतिष्ठित परिवार अपनी कन्याओं और स्त्रियों के जीवन पर विशेष ध्यान देते थे। आगे चलकर कन्यादान पिता का महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य मान लिया गया। नगरीकरण के साथ विचारों का आदान-प्रदान तेज हो गया। इसके फलस्वरूप आरम्भिक आस्था और विश्वासों को मान्यता मिलनी कम हो गयी तथा लोगों ने स्वयंवर प्रथा को अपना लिया।
5. धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के आठ प्रकार मान्य हैं। इनमें से प्रथम चार ‘उत्तम’ माने जाते थे और शेष को निंदित माना गया। सम्भवतः ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणीय नियमों को नहीं मानते थे।
6. ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार स्त्रियों का गोत्र पति का गोत्र माना जाता था। सातवाहन वंश में इस प्रथा को नहीं माना गया और पत्नियों ने अपने पिता के गोत्र को जारी रखा।
इस पोस्ट में Class 12th History Chapter 3 बंधुत्व,जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज Notes in Hindi बंधुत्व जाति तथा वर्ग नोट्स बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज प्रश्न उत्तर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के प्रश्न उत्तर pdf इतिहास कक्षा 12 वीं अध्याय 3 notes बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज MCQ इतिहास कक्षा 12 वीं अध्याय 3 Question Answer kinship, caste and class question answer Kinship Caste and Class with notes in hindi बंधुत्व, जाति तथा वर्ग question answer से संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है यह जानकारी फायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके बारे में आप कुछ जानना यह पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछे.